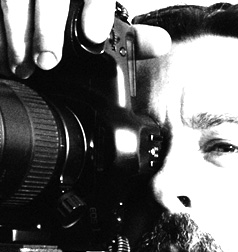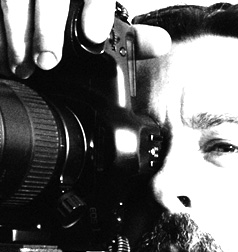आज़ादी के कई दशकों बाद भी, सामाजिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों के बोझ तले दबी भारतीय महिलाएं अपनी स्वतंत्र पहचान साबित करने के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं. भले ही व्यावसायिक तौर पर वे कई ऊंचे मुकाम हासिल करती आई हों, लेकिन हमारा रुढ़िवादी समाज आज भी उन्हें एक असहाय और अबला के रूप में ही देखता है. यह वो समाज है जो लड़की के जन्म को एक अभिशाप मानता है और पैदा होते ही उसकी हत्या कर देना अपनी परंपरा समझता है. हालांकि समय बदलने के साथ ऐसी कुप्रथाओं पर कुछ हद तक विराम जरूर लगा है. अब लड़कियों को पैदा होते ही नहीं मार दिया जाता, बल्कि उन्हें इस कदर शोषित किया जाता है कि उनका जीवन ही उनके लिए मजबूरी बन जाता है.
हमारा पुरुष प्रधान समाज एक महिला को केवल पराश्रित के रूप में ही देखता है, जिसे किसी न किसी रूप में एक पुरुष के सहारे की आवश्यकता जरूर पड़ती है. विवाह से पहले उसे अपने पिता के आदेशों का पालन करना पड़ता है, वहीं विवाहोपरांत वह अपने पति के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हो जाती हैं और उसी के आदेशानुसार जीवन यापन करती हैं. चूंकि स्त्री को बचपन से ही दासता युक्त जीवन जीने की आदत डाल दी जाती है और उसे बचपन से यही ![]() दिखाया जाता है की वो शादी से पहले पिता भाई की गुलाम है और शादी के बाद पति की, इसलिए उसे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पीड़ा नहीं देते. एक ही परिवार में जन्में लड़के और लड़की की परवरिश को भिन्न रखा जाता है. लड़के को केवल आदेश देना और शासन करना सिखाया जाता है, वहीं लड़की को एक आश्रित की भांति आदेश का पालन करना बताया जाता है. जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाती है जो उसे विवाह योग्य बनाने में काफी हद तक सहायक रहता है, जिससे विवाह के पश्चात उसे अपने पति का दुर्व्यवहार बुरा न लगे और वह मरे हुए संबंधों को ढोने लायक बनी रहे. दिखाया जाता है की वो शादी से पहले पिता भाई की गुलाम है और शादी के बाद पति की, इसलिए उसे अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पीड़ा नहीं देते. एक ही परिवार में जन्में लड़के और लड़की की परवरिश को भिन्न रखा जाता है. लड़के को केवल आदेश देना और शासन करना सिखाया जाता है, वहीं लड़की को एक आश्रित की भांति आदेश का पालन करना बताया जाता है. जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाती है जो उसे विवाह योग्य बनाने में काफी हद तक सहायक रहता है, जिससे विवाह के पश्चात उसे अपने पति का दुर्व्यवहार बुरा न लगे और वह मरे हुए संबंधों को ढोने लायक बनी रहे.
विवाह को हमारे समाज में एक ऐसी सम्मानित संस्था का दर्जा दिया गया है, जो केवल एक स्त्री और पुरुष को ही आपस में नहीं जोड़ती बल्कि दो परिवारों को भी एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है. वैवाहिक संस्कारों के नाम पर एक स्त्री को विभिन्न प्रतीकों जैसे मंगलसूत्र, सिंदूर आदि को अपनाने का फरमान जारी कर दिया जाता है, जिसका पालन वह आजीवन करती है. इसके अलावा विवाह के पश्चात एक महिला को अपने पिता के सरनेम को छोड़ पति के सरनेम को भी अपनाना पड़ता है, ताकि वह पूर्ण रूप से अपने पति की संपत्ति बन सके. इसके विपरीत हमारा समाज एक विवाहित पुरुष के लिए ऐसे किसी भी पहचान को जरूरी नहीं समझता. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गृहस्थ जीवन हो या फिर राजनीति, जिसकी प्रधानता होती है, नियम भी केवल उसी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं. अब भला हमारा पुरुष प्रधान समाज किसी ऐसे नियम का निर्माण क्यों करे जो आगे चलकर उसी की स्वतंत्रता की राह में बाधक बन जाए? महिलाएं जिन वैवाहिक प्रतीकों को अपने संस्कार और पहचान समझ कर अपना लेती हैं, अमूमन वही उनकी दासता और शोषण से भरे जीवन को और मजबूत कर देते हैं..
नौकरी के बेहतर अवसरों की तलाश में जब कोई पुरुष अपनी गृहस्थी को छोड़ किसी और शहर में काम ढ़ूंढने जाता है तो ऐसी कोई पहचान उसके साथ नहीं चलती, जिससे यह पता किया जा सके कि वह पुरुष विवाहित है या नहीं. इसी का लाभ उठाकर वह मनचाहे ढंग से अपना जीवन जीने लगता है, स्वय़ं को वह एक अविवाहित की भांति समाज के सामने प्रस्तुत करता है. वह पुरुष जो पूरी तरह से शहरी रंग-ढंग को अपना चुका होता है उसकी पत्नी दिन-रात उसकी खैरियत की फिक्र करती रहती है. लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पडता, क्योंकि वह अपने आप को परिवार का मालिक समझता है, जो जैसे चाहे वैसे जीवन यापन कर सकता है और उससे सवाल करने का अधिकार किसी को नहीं है.. ऐसे वैवाहिक प्रतीकों ने समाज में अपना एक ऐसा स्थान बना लिया है जिससे पार पाना अत्यंत कठिन है. परंपरा के नाम पर हमारा दकियानूसी विचारों वाला समाज एक विवाहिता महिला जिसने सिंदूर न लगाया हो या मंगलसूत्र न पहना हो, उसे सम्मानित नज़रों से नहीं देखता और ऐसी मन्यता भी है कि इनका त्याग केवल पति की मृत्यु के पश्चात ही किया जा सकता है.
हमारे समाज में इन प्रतीकों की उपयोगिता और महत्व इस हद तक बढ़ चुका है कि इनसे अलग एक विवाहित महिला की पहचान स्वत: लुप्त हो जाती है. यद्यपि भारत आधुनिकता की दौड़ में शामिल हो चुका है, लेकिन ऐसे किसी मसले का हल ढ़ूंढ़े से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी मानसिकता ही इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि आज हम झूठे आडंबरों और खोखली मर्यादाओं के जाल में इस कदर उलझे हुए हैं कि इनके सामने व्यक्तिगत इच्छाओं और हितों का कोई महत्व नहीं रह पाता.
भारतीय समाज एक ऐसा रूढ़िवादी समाज है, जो स्वयं ही महिलाओं और पुरुषों को दोहरा जीवन जीने के लिए बाध्य़ कर रहा है. यह काफी हद तक दोनों के, खासतौर पर महिलाओं के सामाजिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है.
यहां प्रश्न यह उठता है कि जब संविधान द्वारा हमें समान राजनैतिक अधिकार मिल सकते हैं तो सामाजिक अधिकारों का बंटवारा समान रूप से क्यों नहीं किया जा सकता?
कभी परंपरा के नाम पर तो कभी रीति-रिवाजों के नाम पर महिलाओं को आए दिन नए-नए तरीकों से यह जताया जाता है कि उनकी पहचान समाज में एक आश्रित से अधिक कुछ नहीं है, और वह खुशी-खुशी ऐसी मान्यताओं को अपना भी लेती हैं. इसके उलट अगर कोई उनकी खराब पारिवारिक हालातों के लिए, या उन पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश भी करता है, तो वह खुद ही उसका समर्थन नहीं करतीं. हजारों वर्षों से चली आ रही दासता उनके दिमाग में ऐसे बैठ चुकी है कि वह अपने परिवार की तथाकथित मान-मर्यादा को अपनी शान समझती हैं. ऐसा नही है कि महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर होती हैं या फिर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय लेने के लिए वे सक्षम नहीं हैं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि बचपन से ही एक लडकी को दासता में जीने की आदत डाल दी जाती हैं, जिसका वह आजीवन पालन करती हैं, और इन सामाजिक बेड़ियों को वह अपनी पहचान मानने लगती हैं. एक तरफ तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल भी हुई हैं, तो फिर ऐसे में उन्हें किन्हीं वैवाहिक प्रतीकों का गुलाम बन कर जीवन यापन करना पड़े, यह बात थोड़ी अटपटी प्रतीत होती है.
|