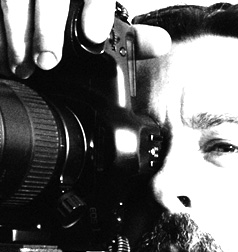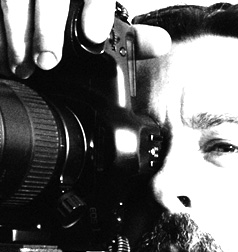जब भी व्यक्ति के चारित्रिक या मानसिक सुधार की बात आती है तो बिना किसी ठोस आधार के हम ऐसा मानकर चलते हैं कि सुधार करने के उद्देश्य से दंड देना अनिवार्य और प्रभावकारी है. जब तक व्यक्ति को उसकी सजा के हिसाब से दण्डित नहीं किया जाएगा तब तक वह कभी भी अपनी गलती को पहचान नहीं पाएगा.
दंड की यह प्रक्रिया बचपन से ही व्यवहारिक रूप ग्रहण कर लेती है. जब बच्चा कोई गलती करता है तो माता-पिता उसे समझाने की बजाए उस पर हाथ उठा देते हैं. कभी-कभार अभिभावक बच्चे को उसकी गलती का अहसास दिलवाने के लिए अन्य लोगों के सामने ही उसे डांटने या मारने लगते हैं. कोई भी माता-पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते इसीलिए इस कदम के पीछे उनका यही उद्देश्य रहता है कि बच्चे को यह समझ आए कि उसने क्या गलत किया है ताकि आगे जीवन में कभी भी वो ऐसी हरकत ना करे.
अध्यापकों की मानसिकता भी दंड के इसी नियम पर केन्द्रित रहती है. अगर छात्र स्कूल में कोई गलती करें या दिया गया काम समय पर पूरा ना करें तो वह उन्हें शारीरिक दंड देना ही बेहतर समझते हैं. क्लास के अन्य बच्चों के सामने उस पर हाथ उठा कर उन्हें लगता है बच्चे को सही राह पर ले जाने का उनका उद्देश्य पूरा हो गया.
लेकिन क्या ऐसे बच्चे जो अपनी हर छोटी गलती के लिए अभिभावकों और अध्यापकों के क्रोध का शिकार बनते हैं आगे चलकर एक अच्छे सामाजिक नागरिक बन सकते हैं?
अक्सर देखा जाता है कि जिन बच्चों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है वह आगे चलकर असामाजिक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं और अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए परेशानी बन जाते हैं. पहले वह अपने अभिभावकों और अध्यापकों को परेशान करते थे अब वह अपने समाज के लिए एक खतरा बन जाते हैं. उनके मन में एक बात बैठ जाती है अगर वह पकड़े गए तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें शारीरिक दंड ही तो दिया जाएगा जिसकी उन्हें अब आदत पड़ चुकी होती है. यही मानसिकता उनसे हर गलत काम करवाती है और जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होता. इस व्यवहार के बच्चे अत्याधिक क्रोधी और जिद्दी बन जाते हैं. उन्हें सही राह पर लाना लगभग असंभव हो जाता है.
बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं. अगर हमारे भविष्य की नींव ही खराब हो या नैतिक विचारों से पूरी तरह दूर हो तो हम कैसे एक सुखद भविष्य और प्रगतिशील समाज की कल्पना कर सकते हैं.
स्कूल और घरेलू मसलों को छोड़ भी दें तो हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भारतीय जेलों को आपराधिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संस्थान माना जाता है. जब एक छोटा सा चोर जेल जाता है तो वहां से निकलने के बाद वह एक शातिर अपराधी बन जाता है. इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण जेल में उसके साथ किया गया कठोर और अमानवीय व्यवहार ही होता है. अगर उस चोर को जेलकर्मियों द्वारा मारा-पीटा ना जाता बल्कि मनोवैज्ञानिक सहायता और पूरी परिपक्वता के साथ उसे अपनी गलती का अहसास करवाया जाता तो शायद वह इस बात को समझ सकता था कि चोरी करना एक अनैतिक काम है. लेकिन सजा देकर हम कैसे किसी व्यक्ति के भीतर चारित्रिक सुधार विकसित कर सकते हैं. एक बार अपराध के क्षेत्र में कदम रखने के बाद व्यक्ति को सजा या दंड का भय नहीं रहता. क्योंकि अगर उन्हें ऐसा कोई भय होता तो वह कभी भी यह राह नहीं चुनते.
वैसे तो यह बात हमेशा से ही विवाद और बहस का विषय रही है कि क्या दंड से सुधार संभव है या नहीं? अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो यह बात स्पष्ट है कि दंड और सुधार कभी साथ-साथ चल ही नहीं सकते. दंड आपराधिक वारदातों और इसके पीछे की सोच को और अधिक मजबूत बनाता है. अगर हम दंड देते हैं तो हमें सुधार की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए.
परिवार और स्कूल का सकारात्मक वातावरण ही बच्चे के भीतर सही सोच और समझ विकसित करता है. गांधी जी जिन्होंने अहिंसा को ही अपना परम धर्म स्वीकार कर लिया था उनका कहना था कि दंड और अहिंसा कभी साथ-साथ नहीं चल सकते. सुधार करने का अर्थ यह कभी नहीं हो सकता कि बच्चे को मारा या प्रताड़ित किया जाए. अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा दी गई नैतिक शिक्षा ही बच्चे के भीतर चारित्रिक गुणों का विकास करती है. बचपन में दी गई सीख ही आगे के जीवन में सही-गलत की पहचान करना सिखाती है. न्याय संस्था या नियम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की सोच व उसकी दूषित मानसिकता को बदलने में कामयाब हो. शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर व्यक्ति को सिर्फ जटिल और जिद्दी ही बनाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप उसके आपराधिक चरित्र को और अधिक बढ़ावा मिलता है.