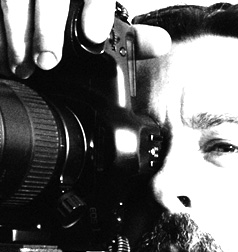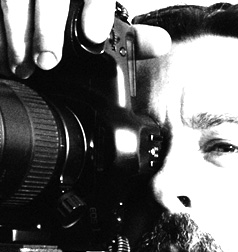सड़क हो या रेल की पटरी या फुटपाथ हो हम सभी ऐसे अनाथ बच्चों को देखते हैं, जिनमें से कुछ तो अपनी मर्जी से घर से भागे होते हैं तो कुछ पारिवारिक कलह की वजह से बाहर रहना पसंद करते हैं तो कुछ भगवान की कोप दृष्टि को भुगत रहे होते हैं. इन बच्चों को हम आम भाषा में "आवारा बच्चे” कहते हैं. वैसे इस क्षेत्र में वह बच्चे भी आते हैं जो 14 वर्ष से कम हैं और बसों और रेल आदि में छोटे-छोटे सामान बेच कर आजीविकार्जन करते हैं. वैसे तो देखने में यह बच्चे खुश नजर आते हैं मगर सच्चाई समाज के सामने आ ही जाती है. इन बच्चों का जीवन किस कदर शोषण और बुराई से घिरा रहता है इसकी खबरें आती रहती हैं. यह बच्चे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के शोषण का शिकार होते हैं.
सडकों पर रहने वाले बच्चे एक ओर जहां दिन भर सूरज की गर्मी में रहते हैं वहीं रात का अंधेरा गुनाह की रोशनी लेकर आता है. यह बच्चे तो सोते हुए भी सुरक्षित नहीं रहते. रेल की पटरियों पर रहने वाले बच्चों को आप हमेशा सस्ते नशे में डूबे पाएंगे और यह शारीरिक शोषण के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं. कुछ ऐसा ही हाल बसों या रेल आदि में घूमने वाले बच्चों का होता है.
सुन के बहुत बुरा लगता है कि जिन बच्चों को हम कल का भविष्य बताते हैं वह इस तरह खराब हो रहे हैं. वह प्रतिभा जिसे देश के काम आना चाहिए वह नित नए जुर्म करता जा रहा है. मासूम बच्चों के साथ होनी वाली शारीरिक उत्पीड़न की घटनाएं तो मन को झकझोर कर रख देती हैं.
इस दुर्दशा के पीछे जितना जिम्मेदार माता-पिता की बेपरवाही है, उतना ही सरकार का ढुलमुल रवैया भी है. कुछ अभिभावक बच्चों की वह देखभाल नहीं कर पाते जो करनी चाहिए तो कुछ उन्हें भगवान भरोसे ही छोड देते हैं. कुछ बच्चे अच्छे भविष्य की चाह में घर से भाग जाते हैं और बाद में उन्हें ऐसी जिन्दगी मिलती है जो इन्हें एक बुरे सपने की याद दिला देता है.
लेकिन अब सवाल उठता है कि जो सरकार महिलाओं के उद्धार के लिए कानून बना रही है, जो सुप्रीम कोर्ट बेवजह के गे-कानून, लिव-इन कानून आदि लागू करने में लगा है क्या उसे इस देश की सबसे बड़ी धरोहर का कुछ ख्याल है. इनके बारे में सरकार और कानून क्या कर-कह रहे हैं और यह कितना कारगर है.
क्या किया जा रहा है स्ट्रीट चाइल्ड के हित में
कानून की बात करें तो इसकी किताब में इनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई कानून हैं. मगर वस्तुस्थिति यह है कि भारत में कानून सिर्फ नाम के होते हैं और इन्हें तोड़ना कोई गलत काम नहीं होता.
26 दिसम्बर 2006 को चर्चा में आए निठारी कांड की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास का सबसे तीखा बयान देते हुए देश की कानून व्यवस्था को बच्चों के प्रति सचेत रहने को कहा, साथ ही उसने ऐसे सभी कानूनों और प्रस्तावों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया जो आवारा या बेसहारा बच्चों की मदद कर सकते थे. इसी कड़ी के कुछ कानून निम्नवत हैं:
एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)
इस स्कीम के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है. इस व्यापक योजना में आपात-कालीन आउटरीच (अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर) सेवाएं, आश्रय, पालन-पोषण, विशेष आवास, खोए और बिछुड़े बच्चों हेतु वेबसाइट और अन्य अनेक नवाचारी हस्तक्षेप सहित बच्चों को सहायता पहुंचायी जाती है.
इस स्कीम के तहत बेसहारा, आवारा, भिखारियों और यौनकर्मियों के बच्चों, मलिन बस्तियों और अन्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया गया है.
इस स्कीम का उद्देश्य योजना कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की देखभाल में सुधार लाने के साथ-साथ उन कार्यों और स्थितियों से जुड़े जोखिमों को कम करना है जो बच्चों के साथ गलत व्यवहार, तिरस्कार, शोषण, उपेक्षा और अलगाव को बढ़ावा देते हैं. एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम में उन बच्चों पर ध्यान दिए जाने का प्रावधान है जिनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है साथ ही उन बच्चों के संरक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया गया है जिनकी प्रायः कानून के साथ खींचतान चलती रहती है अथवा उससे सामना करना पड़ता है.
आईसीपीए न सिर्फ वंचित और खतरों के बीच रहने वाले परिवारों के बच्चों, आवारा बच्चों, अल्पसंख्यकों के बच्चों, एचआईवीएड्स पीड़ित या प्रभावित बच्चों, अनाथ, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों, बाल भिखारियों, यौनशोषित बच्चों, तथा कामकाजी बच्चों तक ही सीमित नहीं है बल्कि कानून के अनुसार यह सभी बच्चों पर लागू होता है जो किसी भी प्रकार के शोषण से ग्रसित है.
आईसीपीएस के अंतर्गत सभी बाल संरक्षण कार्यक्रम आते हैं. इनमें बाल न्याय कार्यक्रम, आवारा बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम, स्वदेशी दत्तक ग्रहण प्रोत्साहन हेतु शिशु गृहों को सहायता जैसे कार्यक्रम भी शामिल हैं. आईसीपीएस में शामिल पहले के कार्यक्रमों में कुछ अतिरिक्त सुधार और संशोधन भी किए गए हैं. इस कानून के अलावा भी कई कानून है जो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए बनाए जाते है, जैसे समन्वित बाल विकास सेवा योजना, उदिशा, एकीकृत स्ट्रीट चाइल्ड प्रोगाम.
समन्वित बाल विकास सेवा योजना
यह पूरे देश में या यों कहे विश्वाभर में, बाल विकास के संबंध में, अत्यकधिक व्यांपक योजनाओं में से एक है. बच्चोंद के संबंध में राष्ट्री य नीति के अनुसरण में महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को 1975 से चलाया जा रहा है. इसका उद्देश्यस स्कूाल जाने से पहले बच्चों के लिए एकीकृत रूप से सेवाएं उपलब्धा कराना है, ताकि ग्रामीण, आदिवासी और झुग्गी वाले क्षेत्रों में बच्चों की उचित वृद्धि और विकास सुनिश्चिरत किया जा सके. इस केन्द्र प्रायोजित योजना द्वारा बच्चों के पोषण की निगरानी की जाती है.
एकीकृत स्ट्रीट चाइल्ड प्रोगाम
सबसे कारगार योजना है एकीकृत स्ट्रीट चाइल्ड प्रोगाम जिसके अंतर्गत बच्चों को सारे दिन छ्त मुहैया कराई जा रही है, उन्हें तकनीकी शिक्षा दी जा रही है आदि.
उदिशा
यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त महिला व बाल विकास परियोजना है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में बाल देखभाल करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है.
पर क्या यह कानून काफी है. भारत में इतने कानूनों के बाद भी इन बच्चों की दशा दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है. चाहते हुए भी सरकार इस समस्या पर काबू नहीं कर पा रही है तो इसका प्रमुख कारण है समाज का साथ न देना. जी हां, सरकार को दोष देना या कानूनों का रोना अब बंद होना चाहिए.
इस क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों ने सबसे ज्यादा काम किया है क्योंकि इनकी पहुंच हर तबके तक है. गैर-सरकारी संगठनों के काम को न सिर्फ आम जनता बल्कि सरकार ने भी बहुत सराहा. इनके अथक प्रयासों की वजह से ही थोड़ी-बहुत हालत सुधरी है.
जरूरत है तुरंत चेतने की
जिस अंदाज में गैर सरकारी संस्थानों ने बच्चों की मदद की है उससे यह साफ हो गया है कि स्ट्रीट चाइल्ड या आवारा बच्चों की मदद करने के लिए बिलकुल निम्नतम स्तर पर जाना होगा तभी कुछ संभव है वरना सरकार के नुमाइंदे तो बाहर ही देखते रहेंगे और इन बच्चों का भला नहीं हो पाएगा.
अगर अब हम नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब यही आवारा बच्चे अपने ही समाज के लिए खतरा बन जाएंगे क्योंकि यह तो हम जानते ही हैं कि बच्चे उस कोमल पंख की तरह होते हैं जो हवा के साथ बह जाते हैं. जिस तरफ हवा होगी उसी ओर यह बच्चे बह चलेंगे.
कानूनों और सरकार की जिम्मेदारी को उन्हीं के ऊपर छोड दें और आगे से जब भी किसी बच्चे को आवारा देखें तो 1098 जो कि भारत में बच्चों की हेल्पलाईन है, फोन कर उन्हें इस बारे में जानकारी दें. साथ ही अपने आस-पास भी जागृति फैलाएं ताकि समाज स्वयं अपनी भी जिम्मेदारियों को समझ सके.
जिस अंदाज में गैर सरकारी संस्थानों ने बच्चों की मदद की है उससे यह साफ हो गया है कि स्ट्रीट चाइल्ड या इन आवारा बच्चों की मदद करने के लिए बिलकुल छोटे स्तर पर जाना होगा तभी कुछ संभव है वरना सरकार के नुमाइंदे तो बाहर ही देखते रहेंगे और इन बच्चों का भला नही हो पाएगा.